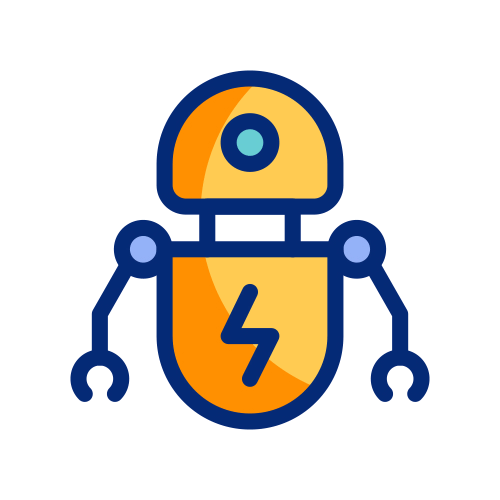कब खत्म होगी अंकों की अंधी दौड़, बच्चों को अंकों की अंतहीन दौड़ में झोंकने के बजाय उनके समग्र व्यक्तित्व विकास पर देना होगा ध्यान
समाज और संस्थाओं को सोचना होगा कि ये बच्चे या विद्यार्थी उत्पाद न होकर जीते-जागते मनुष्य हैं और मनुष्य का निर्माण स्नेह समर्पण त्याग संयम धैर्य सहयोग समझ एवं संवेदनाओं से ही संभव है। ध्यान रहे कि मनुष्य का मनुष्य हो जाना ही उसकी चरम उपलब्धि है। इसलिए अपनी संततियों को अंकों की अंतहीन दौड़ में झोंकने के बजाय उनके समग्र संतुलित व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देना चाहिए।

प्रणय कुमार। बीते दिनों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने दसवीं एवं बारहवीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। तमाम बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम आते ही इंटरनेट मीडिया से लेकर पास-पड़ोस तक कहीं बधाइयों का तांता लगा है तो कहीं शोक का सन्नाटा पसरा है। कोई ठहरकर यह सोचने को तैयार नहीं कि कोई भी परीक्षा जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं होती और न ही किसी एक परीक्षा के परिणाम पर सब कुछ निर्भर करता है। जीवन अवसर देता है और बहुधा बार-बार देता है। अंततः ज्ञान और प्रतिभा ही मायने रखती है और इन्हीं पर जीवन की स्थायी सफलता-असफलता निर्भर करती है।
समाज में प्रायः ऐसे दृष्टांत देखने को मिलते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं में कम अंक लाने या प्रतियोगी परीक्षाओं में मिली प्रारंभिक विफलता के बाद भी धैर्य और निरंतरता के साथ किए गए परिश्रम अंततः फलदायी सिद्ध होते हैं। फिर भी ऐसे तमाम दृष्टांतों के बावजूद बोर्ड एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव में एक ओर गुम होता बचपन दिखाई देता है तो दूसरी ओर येन-केन-प्रकारेण पास होने और अधिक से अधिक अंक बटोरने का असीम उतावलापन भी दिखता है।
सवाल है कि क्या कागज के एक टुकड़े भर से किसी के ज्ञान या व्यक्तित्व का समग्र और सतत आकलन-मूल्यांकन किया जा सकता है? क्या किसी एक परीक्षा की सफलता-असफलता पर ही भविष्य की सारी सफलताएं-योजनाएं निर्भर किया करती हैं? जीवन की वास्तविक परीक्षाओं में ये परीक्षाएं कितनी सहायक हैं? इन्हें जाने-विचारे बिना अंकों के पीछे दौड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।
अधिक प्राप्तांक एवं प्रतिशत को ही सफलता की एकमात्र कसौटी बनाने-मानने से सामाजिकता, संवेदनशीलता, सरोकारधर्मिता, रचनात्मकता जैसे गुणों या मूल्यों की कहीं कोई चर्चा ही नहीं होती। यदि किसी विद्यार्थी के प्राप्तांक कम हैं, लेकिन वह नैतिक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, व्यावहारिक कसौटियों पर खरा उतरता हो तो क्या ये सब उसकी योग्यता के मापदंड नहीं होने चाहिए? क्या उसके संवाद कौशल, नेतृत्व क्षमता, सेवा एवं सहयोग की भावना, प्रकृति-परिवेश, स्वास्थ्य-स्वच्छता आदि के प्रति सजगता आदि का आकलन नहीं किया जाना चाहिए?
पिछले सौ वर्षों की महानतम मानवीय उपलब्धियों पर यदि नजर डालें तो मानवता को दिशा देने वाले, बड़े कारनामे करने वाले विद्यालयी परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक लाने वाले लोग नहीं थे, बल्कि उनमें से कई तो तत्कालीन शिक्षण तंत्र की दृष्टि में कमजोर या फिसड्डी थे। हां, समाज को लेकर उनका ज्ञान विशद और दृष्टिकोण व्यापक अवश्य था। अंकों की अंधी दौड़ का हिस्सा बनने से उचित क्या यह नहीं होता कि हम इस पर गंभीर चिंतन और व्यापक विमर्श करते कि क्यों हमारे शिक्षण संस्थान वैश्विक मानकों एवं गुणवत्ता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते?
क्यों हमारे शिक्षण संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में मौलिक शोध एवं वैज्ञानिक-व्यावहारिक दृष्टिकोण का अभाव परिलक्षित होता है? क्यों हमारे शिक्षण संस्थान अभिनव प्रयोगों, नवोन्मेषी पद्धतियों, विश्लेषणपरक प्रवृत्तियों को बढ़ावा नहीं देते? क्यों हमारे शिक्षण संस्थानों से निकले अधिकांश विद्यार्थी आत्मनिर्भर और स्वावलंबी नहीं बन पाते? क्यों उनमें कार्यानुकूल दक्षता एवं कुशलता की कमी देखने को मिलती है? क्यों वे साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों, विषमताओं और प्रतिकूलताओं का सामना नहीं कर पाते?
अंकों की प्रतिस्पर्धा का ऐसा आत्मघाती दबाव दुखद है। इस दबाव में बच्चे सहयोगी बनने की अपेक्षा परस्पर प्रतिस्पर्धी बन रहे हैं। ऐसी अंधी प्रतिस्पर्धा कुछ के अहं को तुष्ट कर उन्हें एकाकी और स्वार्थी बनाती है तो कुछ को अंतहीन कुंठा की गर्त में धकेलती है। और यह तथ्य है कि प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या में व्यक्ति प्रकृति में सर्वत्र व्याप्त सहयोग, सामंजस्य और सौंदर्य को विस्मृत कर बैठता है।
प्रतिस्पर्धा करते-करते वह अपने घर-परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति भी अक्सर प्रतिस्पर्धी भाव रखने लगता है। कई बार तो वह अपनों के प्रति भी कटु और कृतघ्न हो उठता है। यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि हम उसे बचपन से ही दूसरों को पछाड़ने की सीख दे रहे हैं? जबकि हमें साथ, सहयोग और सामंजस्य की सीख देनी चाहिए। ‘जीवन एक संघर्ष है’ उससे कहीं अधिक आवश्यक है, यह जानना-समझना कि जीवन ‘विरुद्धों का सामंजस्य’ तथा ‘सहयोग एवं संतुलन’ की सतत साधना है।
अंकों की गलाकाट प्रतिस्पर्धा वाले इस दौर में सफलता के सब्जबाग दिखाते और सपने बेचते कोचिंग संस्थान कोढ़ में खाज का काम करते हैं। वे अभिभावकों से सफलता का सौदा करते हैं। कई बार तो बहुतेरे अभिभावक अपने बच्चों की रुचि एवं क्षमता का विचार किए बिना अपने सपनों का बोझ जाने-अनजाने उनके कोमल कंधों पर डालने की भूल कर बैठते हैं। यदि वे सफल हुए तो ठीक, लेकिन अगर विफल हुए तो जीवन भर उस विफलता की ग्लानि से बाहर नहीं निकल पाते।
समाज और संस्थाओं को सोचना होगा कि ये बच्चे या विद्यार्थी उत्पाद न होकर जीते-जागते मनुष्य हैं और मनुष्य का निर्माण स्नेह, समर्पण, त्याग, संयम, धैर्य, सहयोग, समझ एवं संवेदनाओं से ही संभव है। ध्यान रहे कि मनुष्य का मनुष्य हो जाना ही उसकी चरम उपलब्धि है। इसलिए अपनी संततियों को अंकों की अंतहीन दौड़ में झोंकने के बजाय उनके समग्र, संतुलित व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देना चाहिए। जीवन बहुरंगी एवं बहुपक्षीय है और हर रंग एवं पक्ष का अपना सौंदर्य, महत्व और आनंद है। हर रंग और पक्ष को हृदय से स्वीकार करने में ही जीवन की सार्थकता है।
(लेखक शिक्षाविद् एवं सामाजिक संस्था ’शिक्षा-सोपान’ के संस्थापक हैं)